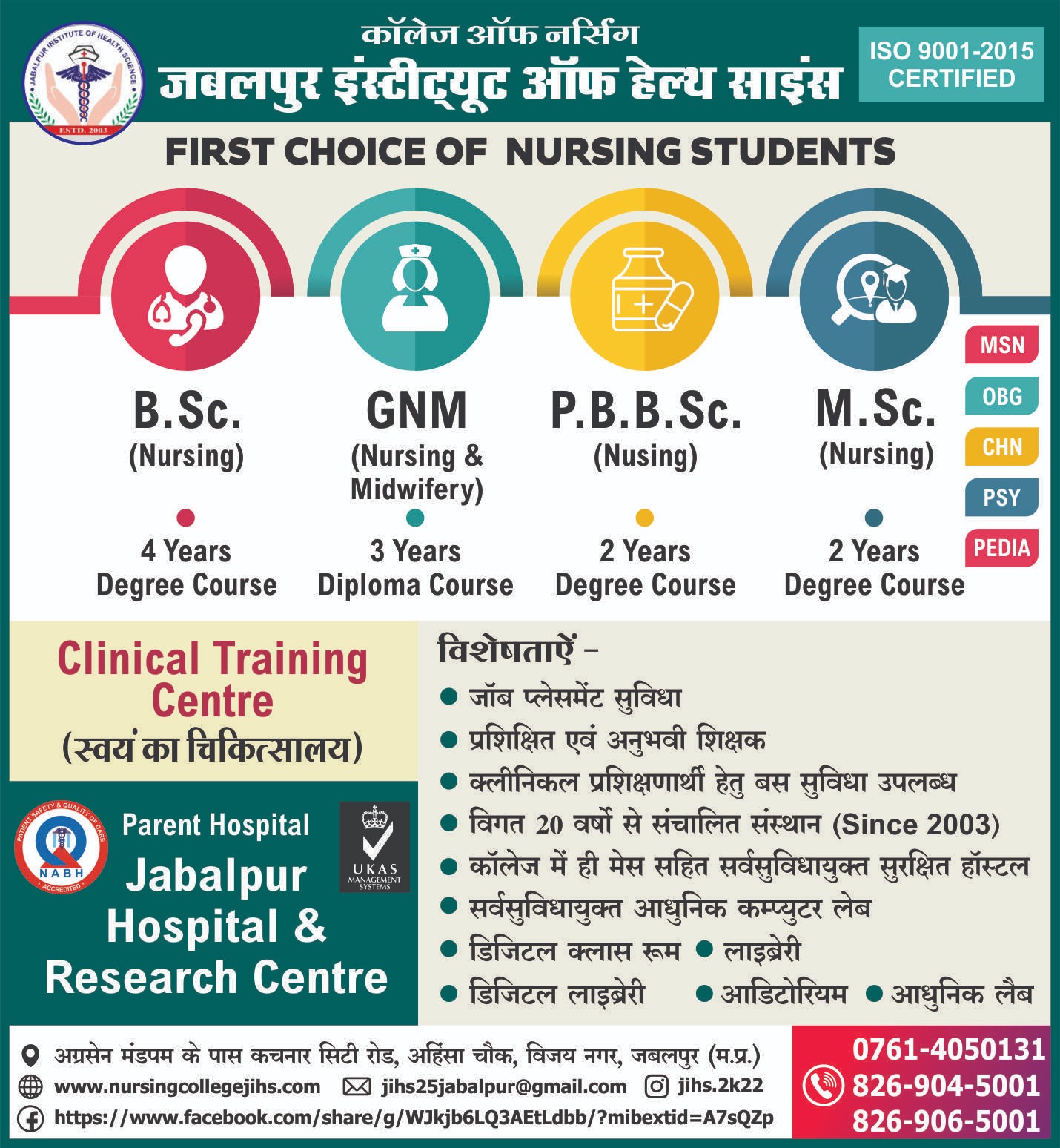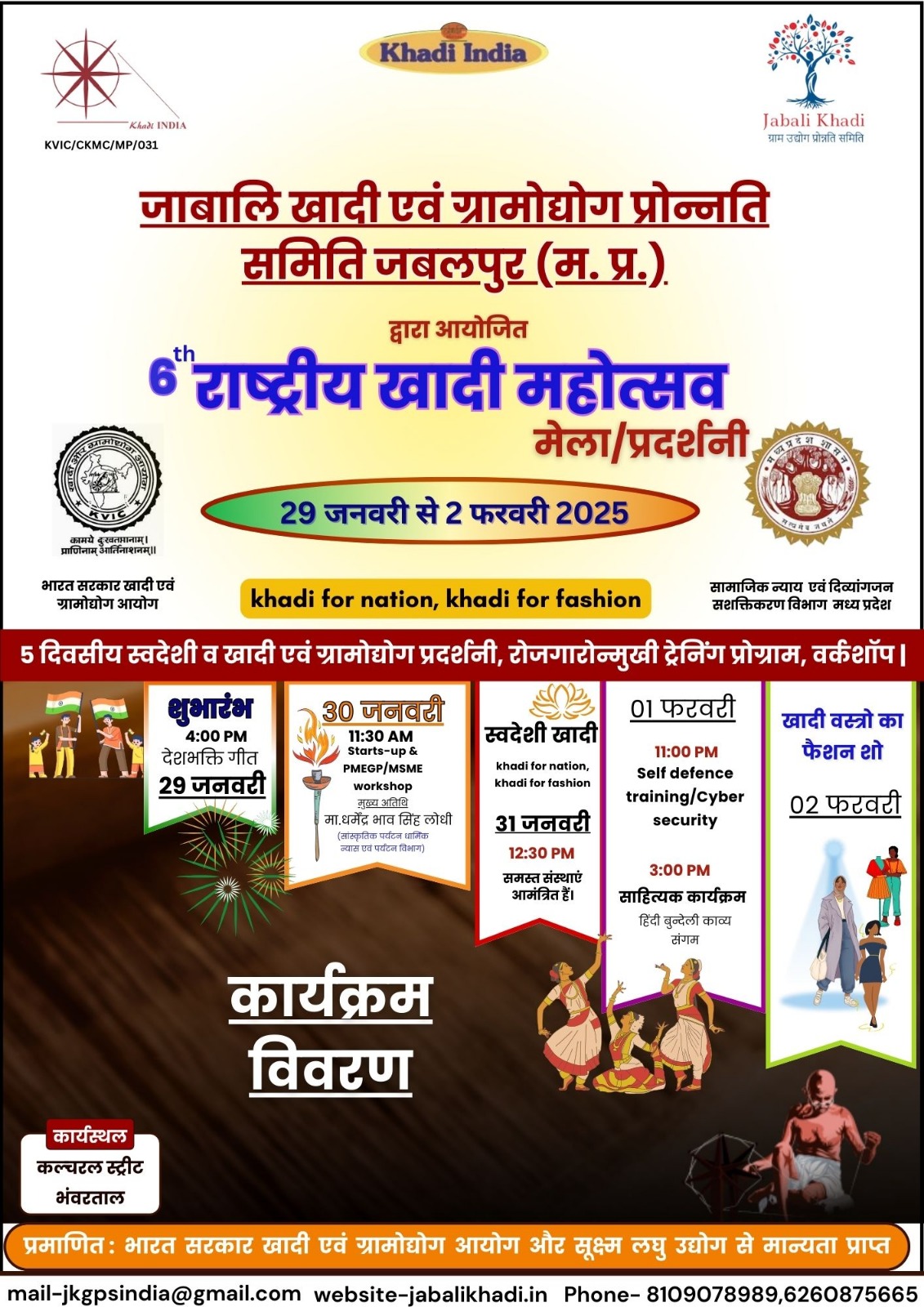प्रिय आत्मन, गीता जयंती पर एक लेख लिख रहा था तो लगा कि 1000 शब्दों में अपनी बात नहीं कह सकता। तब पाँच लेखों की श्रृंख्ला लिखना प्रारंभ किया। इसी बीच विचार आया कि क्यों न इस श्रृंखला को निरंतर लिखा जाए जब तक गीता पूर्ण न हो जाए। इन लेखों को अत्यंत सरल और व्यवहारिक रखने का प्रयास किया गया। प्रत्येक लेख को छोटे-छोटे उप शीर्षकों में बाँटा जा रहा है।
ओम प्रकाश श्रीवास्तव
आईएएस अधिकारी तथा
धर्म और अध्यात्म के साधक
‘गीता को जानें’ लेखमाला- (4)
ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझें
गीता में भगवान् कहते हैं कि वह ज्ञान को विज्ञान सहित (9.1) बता रहे हैं। यहाँ ज्ञान का अर्थ है जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है व मस्तिष्क में संग्रहित रहता है। जैसे हम गीता को पढ़ें, सुनें, बोलें तो हमें ब्रह्म, प्रकृति, योग आदि की जानकारी होगी। यह ज्ञान है। यह ज्ञान इन्द्रियों और मस्तिष्क तक सीमित होता है इसलिए यह स्थाई नहीं है। जब शरीर पीड़ा में होगी, इन्द्रियाँ शिथिल होंगीं तो यह विस्मृत हो जाएगा। कई लोग जीवन भर गीता या किसी अन्य धर्मग्रंथ का पाठ करते हैं, उसे कंठस्थ कर लेते हैं, पर जीवन में मुसीबत आती है, मृत्यु का समय आता है तो उनके भीतर की शांति बिक्षुव्ध हो जाती है। वे बैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा आम संसारी व्यक्ति करता है। इसे ऐसे समझें कि ऐसे लोग भोजन बनाने की विधि तो जानते हैं परंतु उन्होंने भोजन पकाया नहीं है, भोजन कयिा नहीं है। भोजन बनाने की विधि भूख नहीं मटिा सकती । उसके लिए तो भोजन पकाना ही पड़ेगा और उसे खाना पड़ेगा। दूसरी ओर विज्ञान का अर्थ है वह अनुभव जो अंदर उतरता है, जो हमें अंदर से बदल देता है। इसका अर्थ है भोजन कर लेना और भूख मिट जाना। गीता कहती है कि केवल ज्ञान की लम्बी चौंडी बातें करने से कोई पंडित नहीं बन जाता (2.11)। पंडित वह है जिसने इस ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष कर लिया है। हमारा लक्ष्य भोजन की जानकारी ही प्राप्त करना भर नहीं है, हमारा लक्ष्य है भोजन पकाना और उससे अपनी भूख मिटाना। गीता यह दोनों काम करने में हमारा मार्गदर्शन करती है। इसके लिए गीतोक्त जीवन जीना होता है । इसका क्रम से ज्ञान कराना ही गीता का उद्देश्य है। जब गीता का ज्ञान हमारे अंदर की अनुभूति या वज्ञिान बन जाता है तो हम हर सुख दुख में, संसार के झंझावातों में समत्व में जीने लगते हैं। श्रीरामकृष्ण इसके उदाहरण हैं। अंतिम समय में वे मुँह के कैंसर के कारण शारीरिक रूप से अत्यंत कष्ट में थे। जब शिष्यों ने कहा कि आप अपने कष्ट को समाप्त करने के लिए माँ काली से प्रार्थना क्यों नहीं करते। पहले तो वे मना करते रहे। पर जब शिष्यों ने बहुत आग्रह किया तो वे माँ काली के मंदिर में गये। जब बाहर आए तो शिष्यों ने पूछा कि क्या कहा माँ ने। तो रामकृष्ण अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि माँ ने कहा है कि तुम इतने मुखों से खा तो रहे हो। यह उनकी अनुभूति है जिसके सामने शारीरिक कष्ट गौण हो गया है। अत्यंत शारीरिक कष्ट के बाद भी वह समत्व में हैं। गीता के अनुसार संसार में सुख दु:ख तो आएँगे। इन्हें पूर्णत: हटाने का कोई तरीका नहीं है। इन्हें सहन करना है (2.14)। मन और बुद्धि को शांत और सम रखते हुए इनसे जूझना है। इस अंतर को समझ लें तो हमारा लक्ष्य तय हो जाएगा। गीता की पाठशाला में हम पाठ भी सीख पाएँगे और उस जानकारी का अपने जीवन में प्रयोग करते चलेंगे। गीता केवल कंठस्थ करने तक, पूजा करने तक सीमित नहीं रहेगी, वह हमारे अंदर की अनुभूति बन जाएगी।
गीता की टीकाओं का महत्व और सावधानी
गीता पर अनेक टीकाएँ हुई हैं। टीका का अर्थ है गीता के शब्दों और श्लोकों की व्याख्या। गीता सूत्र रूप में है अन्यथा भला 700 श्लोकों में उपनिषदों का अनन्त ज्ञान कैसे समा सकता है उदाहरण के लिए आइंस्टाइन ने परमाणु ऊर्जा की खोज की। उन्होंने सूत्र दिया कि पदार्थ की मात्रा में प्रकाशवेग का दो बार गुणा कर दें तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की गणना हो जाएगी (ष्ट=द्वष्2). इस सूत्र को प्राप्त करने के पीछे जटिल गणितीय समीकरणों का योगदान है। इस सूत्र का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए विस्तृत विधियों की जरूरत होगी। यह गणितीय समीकरण तथा विधियाँ ही उस सूत्र की टीका हैं। शास्त्रीय रूप से देखें तो गीता की तीन श्रेणी की टीकाएँ हैं। श्रीमद् शंकराचार्य ने अद्वैतवादी, श्री मध्वाचार्य ने द्वैतवादी और श्री रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवादी टीका की है। इसके बाद अनेक महापुरुषों ने मोटे तौर पर इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए गीता की व्याख्याएँ की हैं। गीता के विद्यार्थी को प्रारंभ में ही बड़ी-बड़ी टीकाओं में उलझने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं का एक अनुभव बताता हूँ। वर्ष 2003 की बात थी। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मेरे सहयात्री एक युवा संन्यासी थे। मैं गीता पर कोई भाष्य पढ़ रहा था। संन्यासी ने उसके बारे में मुझसे पूछा। तब तक मैं 20 वर्षों का गीतापाठी हो चुका था और गीता के लगभग सभी महत्वपूर्ण भाष्य पढ़ चुका था। अत: मैनें कुछ अहंकार के साथ बताया कि वह पुस्तक क्या है। बात आगे बढ़ी तो मैनें कुछ टीकाओं की तुलनात्मक व्याख्या की। युवा संन्यासी ने मुझसे पूछा कि जब गीता एक है तो उसकी विविध टीकाएँ क्यों हैं। कोई उसमें अद्वैत देखता है तो कोई द्वैत तो कोई उसे केवल कर्म का ग्रंथ मानता है आदि-आदि। मैनें कहा कि जैसे बिजली शुद्ध ऊर्जा है जिसका उपयोग हीटर में गर्म करने के लिए होता है तो रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए। बिजली का उपयोग उपकरण की पात्रता और जरूरत के आधार पर तय होता है । गीता शुद्ध अध्यात्म विज्ञान है। जो व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा उसकी चेतना का स्तर, समझ, स्वभाव जैसा होगा उसी के अनुरूप वह गीता को समझेगा और उपयोग करेगा। युवा संन्यासी बोले बिलकुल ठीक कहा । शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वविेकानन्द जैसे महापुरुष संसार के उद्धार के लिए आते हैं इसलिए उनके समय समाज की जैसी दशा होती है व जैसी जरूरत होती है उसी तरह की टीका उनके द्वारा की गई। इतना कहकर संन्यासी बोले आपकी चेतना का स्तर इनमें से किस टीकाकार के स्तर का है मैं चकरा गया। मैंनें कहा स्वामी जी मैं तो इनमें से किसी के पाँव की धूल भी नहीं हूँ। वह बोले तब तुम टीकाओं को पढक़र क्या समझ पाओगे, जो जानकारी एकत्र करोगे वह उधार की जानकारी होगी। तुम्हारी स्वयं की अनुभूति नहीं होगी। फिर मार्ग बताते हुए बोले कि गीता में संसार के सभी मानवों के लिए उनके स्तर का संदेश निहित है।
गीता को श्रद्धा व विश्वास से पढ़ो। मन में दृढ़ विश्वास रखो कि मेरे अंदर श्रीकृष्ण का निवास है और वही गीता को उच्चारित कर रहे हैं। प्रत्येक श्लोक को देवता मानकर उससे अपना अर्थ देने की प्रार्थना करो। तब गीता का अर्थ आपके हृदय में प्रकट होने लगेगा। टीकाएँ पढऩा बुरा नहीं हैं। वे मार्गदर्शक हैं परंतु मार्ग को जानने मात्र से मंजिल पर नहीं पहुँचा जा सकता। उसके लिए तो चलना पड़ता है। कई बार बहुत ज्यादा पढऩे सुनने से भी मार्गों के बारे में भ्रम हो सकता है। गीता से जुडऩा ही मंजिल की ओर चल पडऩा है और अनुभूति प्राप्त करना ही मंजिल प्राप्त करना है।
कुछ जिलों में पूर्णता शराब बंद ,निर्णय पर कैबिनेट की मोहर : इन स्थानों पर शराब बंदी हुई