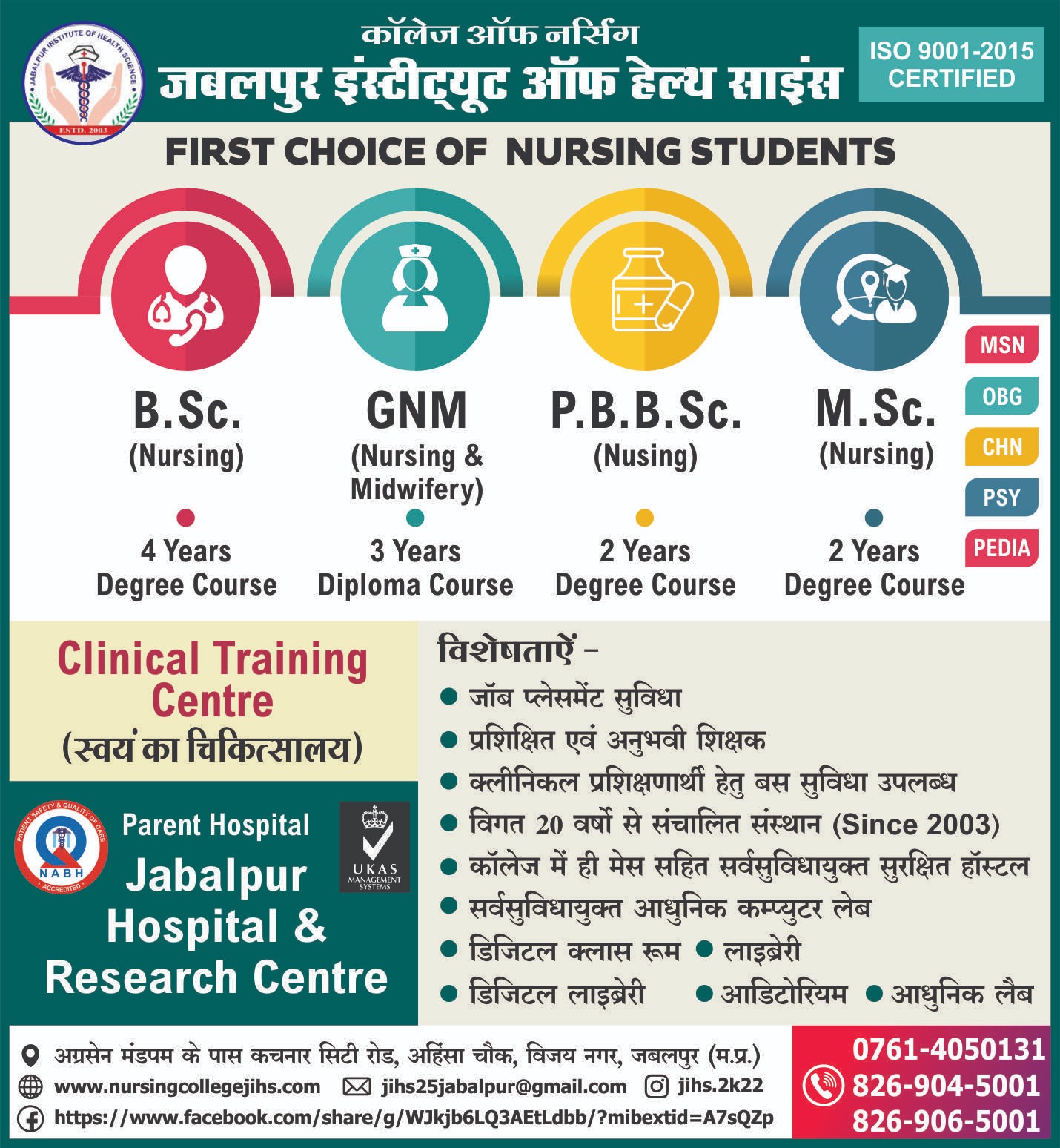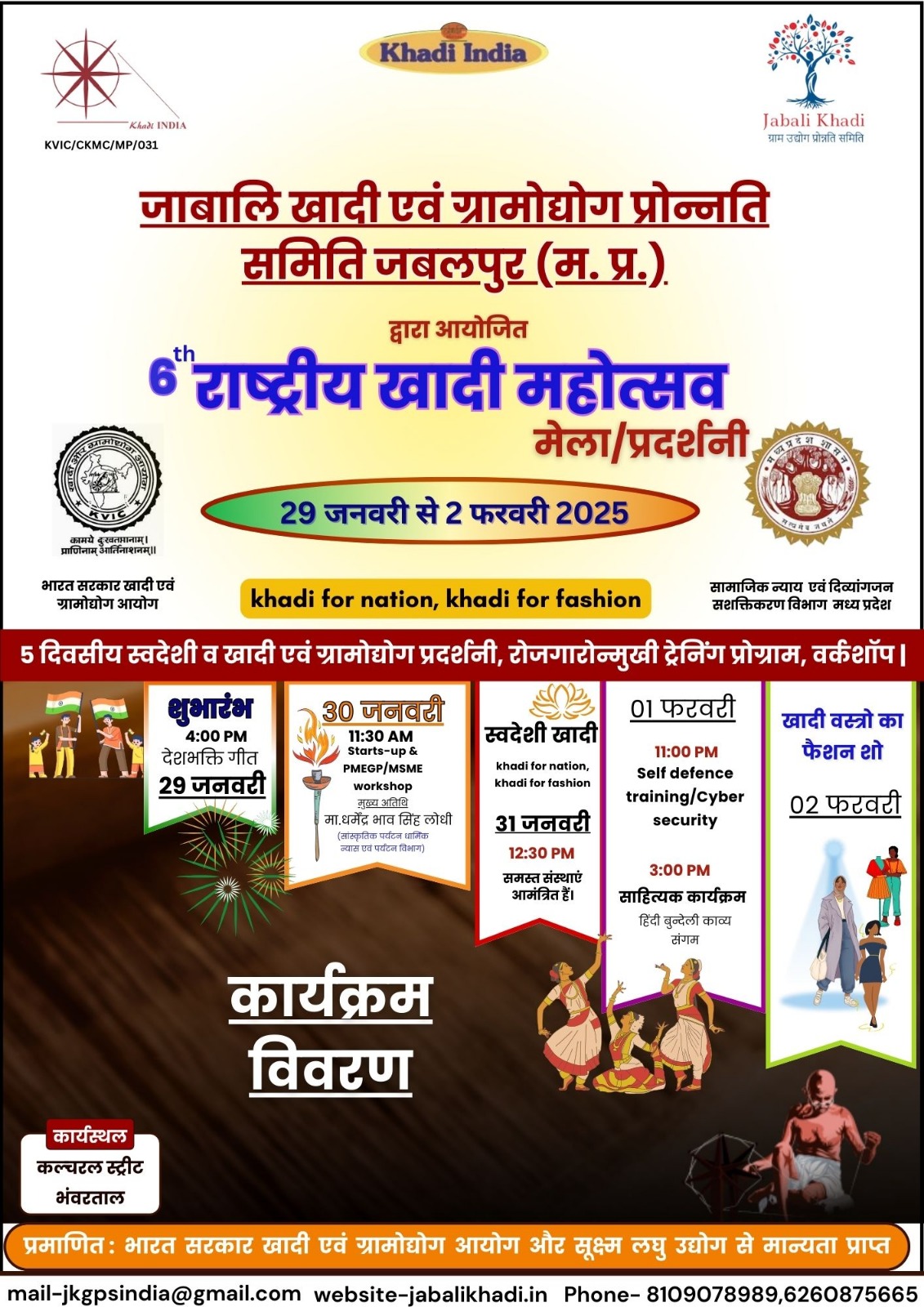प्रिय आत्मन, गीता जयंती पर एक लेख लिख रहा था तो लगा कि 1000 शब्दों में अपनी बात नहीं कह सकता। तब पाँच लेखों की श्रृंख्ला लिखना प्रारंभ किया। इसी बीच विचार आया कि क्यों न इस श्रृंखला को निरंतर लिखा जाए जब तक गीता पूर्ण न हो जाए। इन लेखों को अत्यंत सरल और व्यवहारिक रखने का प्रयास किया गया। प्रत्येक लेख को छोटे-छोटे उप शीर्षकों में बाँटा जा रहा है।
ओम प्रकाश श्रीवास्तव
आईएएस अधिकारी तथा
धर्म और अध्यात्म के साधक
शब्दजाल में उलझने से बचें – गीता का बारम्बार श्रद्धा और भक्ति से पाठ करें और स्वाभाविक ज्ञान से जिस अर्थ का बोध हो उसे ग्रहण करें। प्रारंभ में कोई अर्थबोध नहीं होता हो तब भी पाठ को निरंतर रखें। यह सोचें कि हर काम केवल मतलब से नहीं किया जाता है। कुछ काम बेमतलब दिखाई देते हैं पर इनका परिणाम बाद में मिलता है। गीता के अध्ययन मनन के साथ श्रीकृष्ण के जीवन का अनुसंधान करें। गीता में जिस श्लोक में कठिनाई आती है उसे श्रीकृष्ण के जीवन की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समझें। इसके बाद वह स्थिति आएगी जब आप अपनी चेतना के स्तर, अनुभव के आधार पर अपना विशिष्ट मार्ग तय कर सकोगे। तब उस मार्ग की प्रमाणिक टीकाएँ मार्गदर्शन करेंगीं। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में गीता पर लिखने का चलन चल पड़ा है। हर दिन गीता पर नई पुस्तक बाजार में आ रही है। इनमें अधिकतर अप्रमाणिक हैं जिनके लेखकों को कोई आत्मानुभव नहीं है। यह शब्दजाल है जो वे कॉपी-कट-पेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने गीता के समग्र ज्ञान को केवल प्रबंधन तक सीमित कर दिया है। एक व्यक्ति जीवन भर भी पढ़े तो मुश्किल से 1000 पुस्तकें पढ़ पाएगा, इसलिए अपना समय केवल प्रमाणिक ग्रंथों के अध्ययन को दें। ऐसे लोगों के प्रवचन सुनें जो तपस्वी हैं। वह संन्यासी हो सकता है और गृहस्थ भी परंतु गीता उसके अंदर उतरी हो अन्यथा हम अपना समय भी खराब करेंगे और शब्दजाल में भटक भी जाएँगे।
पहले गीता की शब्दावली की परिभाषा को समझें – हर विषय की, हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। चिकित्सा विज्ञान की अपनी शब्दावली है, इंजीनियरिंग की अपनी, भूगोल की अपनी। इसी तरह अध्यात्म विज्ञान की अपनी शब्दावली है। विद्यार्थी विद्यालयों में कोई भी विषय पढ़ते हैं तो पहले उससे संबंधित परिभाषाएँ सीखते हैं ताकि विषय समझ सकें। गीता को समझने के लिए आध्यात्मिक शब्दावली की प्रारंभिक जानकारी जरूरी है। गीता में ब्रह्म, आत्मा, प्रकृति, पुरुष, जीव, धर्म, यज्ञ, तप, बुद्धि, इन्द्रिय, संन्यास, क्षर, अक्षर, गुण, ज्ञान, विज्ञान, देही, सनातन, निर्मम, निर्वाण, वर्ण आदि अनेक शब्द आते हैं जो सामान्य और विशेष अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। इनका परिचय न होने से साधक वहीं अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिए वेदान्त के प्रकरण ग्रंथों का साथ-साथ अध्ययन करते चलना चाहिए। श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा रचित आत्मबोध, तत्त्वबोध, अपरोक्षानुभूति, मणिरत्नमाला, तथा भजगोविन्दम् ऐसे ही ग्रंथ हैं। यह बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएँ हैं जो इन आध्यात्मिक शब्दावली से परिचय कराती हैं उनकी परिभाषा स्पष्ट कर देती हैं।
गीता में कई शब्दों को विविध अर्थों में उपयोग में लिया गया है। जैसे धर्म शब्द से धर्म के अलावा कर्तव्य भी सूचित किया गया है पर कहीं भी इसका अर्थ हिन्दू, मुसलमान, ईसाई जैसे विभाजन के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है। इसी प्रकार से धर्मयुद्ध शब्द का वह अर्थ नहीं है जिस अर्थ में पश्चिमी जगत में इसका उपयोग हुआ है। ईसाइयों व मुस्लिमों के बीच येरूशलम पर कब्जा करने को लेकर 7 बार युद्ध हुआ । इसे क्रूसेड कहते हैं। यह दो धर्मों के बीच हुआ था इसलिए इसे भी सामान्य भाषा में धर्मयुद्ध कह देते हैं । परंतु गीता के धर्मयुद्ध का वह अर्थ नहीं जो क्रूसेड का है। इसी तरह गीता में संन्यासी का वह अर्थ नहीं है जैसा कि हम साधारणत: संन्यासी को कर्मत्यागी, गेरुआवस्त्रधारी और भिक्षाटन करने वाले व्यक्ति के रूप में समझते हैं। गीता का संन्यासी वह व्यक्ति है जो राग-द्वेष और कामनाओं से मुक्त है(5.3)। संन्यासी वह है जो कर्मफल पर निर्भर नहीं होता (6.1)। इस प्रकार गीता के अनुसार कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि गृहस्थ भी, संन्यासी हो सकता है यदि ऐसे आंतरिक गुण उसके अंदर हैं। लेखमाला में संदर्भ आने पर इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता रहेगा।
गीता स्मृति ग्रंथ है पर उसका विषय श्रुति का प्रतिपादन – कुछ विद्वान गीता को श्रुति मानते हैं कुछ स्मृति और कुछ श्रुति व स्मृति दोनों । श्रुति परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप है जिसका दर्शन मंत्रों के माध्यम से महान ऋषियों को हुआ है। यह ज्ञानस्वरूप परमात्मा का स्वत: प्रकटीकरण है। इसके अलावा जो ग्रंथ महापुरुष द्वारा स्वयं बोला या लिखा जाता है उसे स्मृति कहते हैं। गीता की विषयवस्तु श्रुतियों का ही प्रतिपादन है परंतु वह अवतार द्वारा बोली गई है इसलिए स्मृति की श्रेणी में आती है। गीता में कही गई बातें पूरी तरह अव्यैक्तिक (द्बद्वश्चद्गह्म्ह्यशठ्ठड्डद्य) हैं। गीता कोई नया मत या वाद स्थापित नहीं करती। भगवान् कहते हैं यह तो वही ज्ञान है जो ऋषियों ने अनेक तरह से कहा है (13.4)। भगवान् ने इसे सर्वप्रथम सूर्य को बताया था और बाद में यह मनु और इक्ष्वाकु के माध्यम से आगे चला परंतु दीर्घकाल में यह लुप्त हो गया था इसलिए भगवान् उसे पुन: अर्जुन को कह रहे हैं 4.1-3)।
गीता सर्वसमन्वयी है – गीता किसी एक दर्शन का प्रतिपादन नहीं करती। वह सारे दर्शनों का समन्वय करती है। जो विद्वान हैं, पंडित हैं वे अपने अपने मत या दर्शन का मंडन और दूसरे के मत के खंडन में पूरी बौद्धिक प्रतिभा लगा देते हैं पर जिनको बोध होता है वे समन्वय की बात करते हैं।
रविदास, मीरा, कबीर जैसे कम पढ़े-लिखे पर बोध को पहुँच चुके महापुरुष के मुँह से समन्वय की ही भाषा निकलती है। वे चेतना की ऊँचाई से सब देखते हैं। उन्हें भेद दिखता ही नहीं। गीता सभी की सहायता करती है किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। गीता के लिए न कोई कम है न अधिक। गीता में कर्मयोग और ज्ञानयोग (सांख्य) दोनों ही एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं (5.4)। गीता में साधक के संस्कार, उसकी चेतना का स्तर और परिस्थिति के अनुसार कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग पर बल दिया है और इन तीनों को ध्यानयोग समान रूप से मदद करता है। गीता ने सभी का समन्वय किया है। इसलिए आप किसी भी मत, वाद या सिद्धांत को मानते हों, गीता माता आपको अपने बच्चे की तरह सदैव संरक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर है।
भगवान् ने गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से सारे मनुष्यों को दिया है। अर्जुन हम जैसे सामान्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके प्रश्न हम सबके प्रश्न हैं। जैसे अर्जुन स्वजनों के मोह में फँसा था, पाप-पुण्य की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा था, शोक से बाहर आने का रास्ता नहीं देख पा रहा था, पलायन करने तैयार था वैसे ही हम भी जीवन में भ्रमित रहते हैं। अपने कल्याण का रास्ता नहीं खोज पाते। गीता हमें अपने कल्याण का मार्ग बताएगी, इस विश्वास के साथ, आइए हम गीता में प्रवेश करें। (क्रमश:)