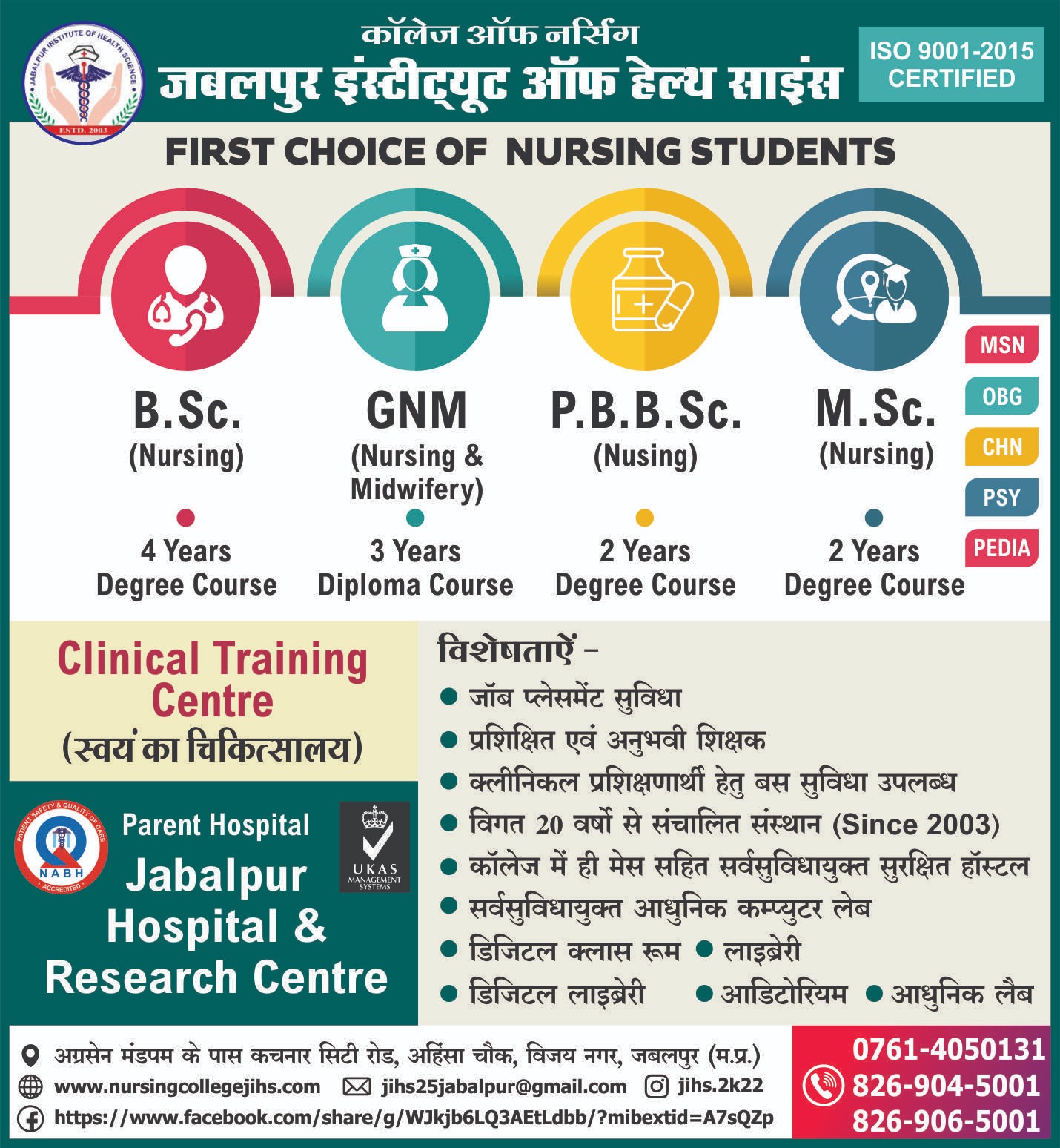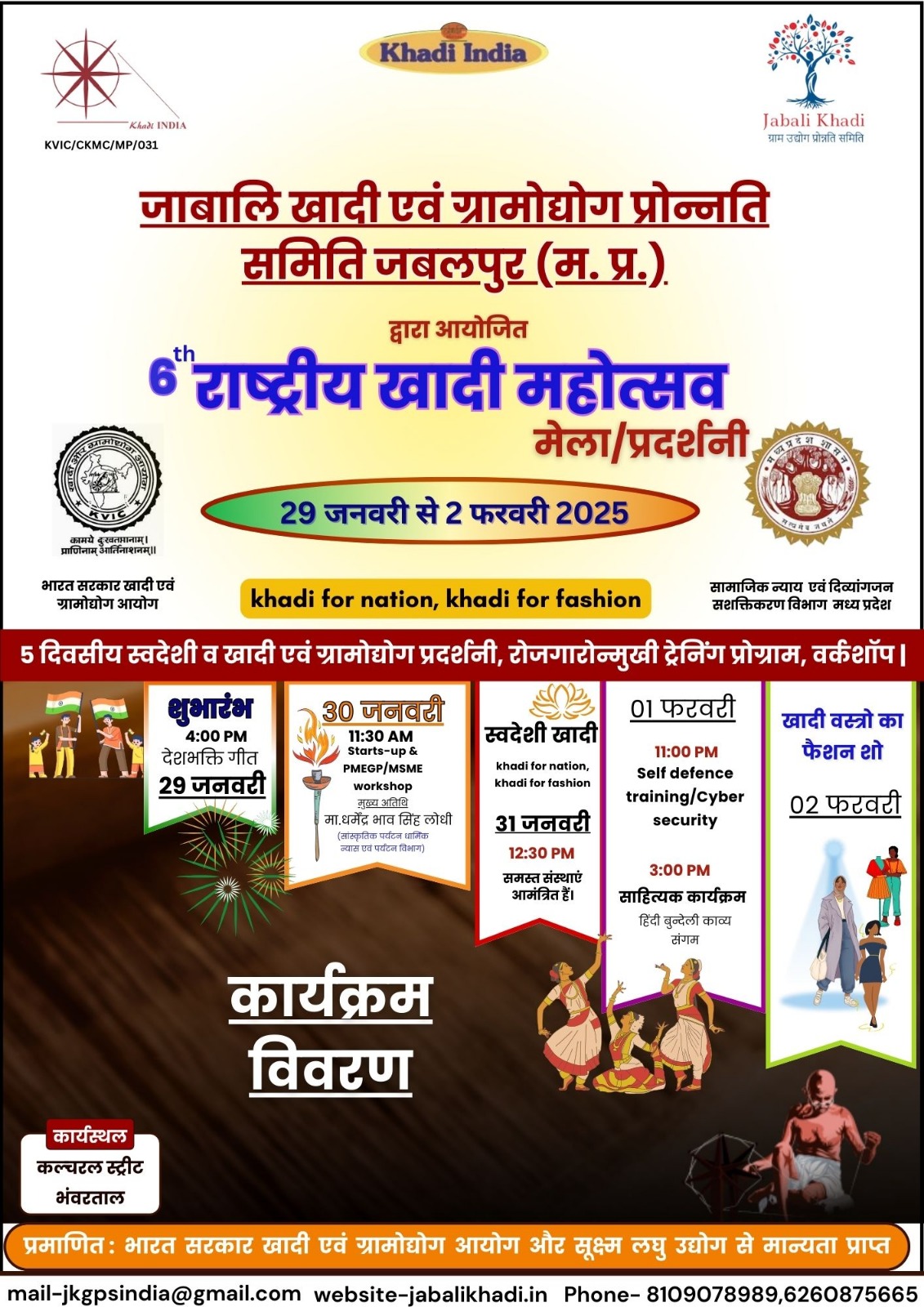प्रिय आत्मन, गीता जयंती पर एक लेख लिख रहा था तो लगा कि 1000 शब्दों में अपनी बात नहीं कह सकता। तब पाँच लेखों की श्रृंख्ला लिखना प्रारंभ किया। इसी बीच विचार आया कि क्यों न इस श्रृंखला को निरंतर लिखा जाए जब तक गीता पूर्ण न हो जाए। इन लेखों को अत्यंत सरल और व्यवहारिक रखने का प्रयास किया गया। प्रत्येक लेख को छोटे-छोटे उप शीर्षकों में बाँटा जा रहा है।
ओम प्रकाश श्रीवास्तव
आईएएस अधिकारी तथा
धर्म और अध्यात्म के साधक
गीता रथ द्वारा आदर्श जीवन का चित्रण –
स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है कि गीता का आदर्श जीवन युद्ध के बीच रथ पर खड़े होकर अर्जुन को गीता का उपदेश देते श्रीकृष्ण के चित्र में प्रदर्शित हुआ है। इस चित्र में अर्जुन धनुष बाण एक ओर फेंक, रथ में कायर की भाँति शिथिल और शोकमग्न होकर बैठा है। सारथी श्रीकृष्ण एक हाथ में चाबुक लिए हैं और उन्होंने दूसरे हाथ से घोड़ों की रास इस प्रकार खींचकर पकड़ रखी है कि घोड़े अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए हैं, उनके अगले पैर हवा में उठे हैं, और मुँह खुल गए हैं। इससे श्रीकृष्ण की छवि में उनकी महान् कर्मशीलता और परिस्थितियों पर पकड़ प्रकट होती हैं। वे अर्जुन की और थोड़ा मुड़ गए हैं, उनके मुख पर स्मित मुस्कान है। उनका शिशु-सरल मुख प्रेम और सहानुभूति से दीप्त हो उठा है और वे अपने अनन्य सखा को गीता का सन्देश सुना रहे हैं। शरीर का एक अंग कार्यरत है और फिर भी मुख पर नील गगन की गंभीर शान्ति और प्रसन्नता व्याप्त है। यही तो गीता का मूल तत्त्व है सब परिस्थितियों में शान्त, स्थिर और अनुद्विग्न रहते हुए – शरीर, मन और आत्मा ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना।
गीताज्ञान सनातन है पर गीता का लेखन ऐतिहासिक है –
विज्ञान के अनुसार 1600 करोड़ वर्ष पूर्व इस संसार के उद्भव के साथ ही विज्ञान के नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण, गति, घर्षण, रासायनिक क्रियाएँ आदि स्वमेव पैदा हो गये थे। पर हम उन नियमों को पिछले 500 वर्षों में समझ तब पाए जब मानव उन्नति के उस सोपान पर पहुँच गया जब उन नियमों को समझने की मानसिक योग्यता वाले लोग पैदा हुए। विज्ञान के नियम हर सृष्टि के लिए अलग-अलग हैं। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम हमारी आकाशगंगा में है वह दूसरी आकाशगंगा में हो यह आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत आध्यात्मिक ज्ञान सर्वत्र और सदैव एक सा है। हर प्रलय के बाद नई सृष्टि में ईश्वर उसे ब्रह्मा के मुख से प्रकट करते हैं। महान ऋषि उस ज्ञान का मंत्रों के रूप में दर्शन करते हैं और वही वेदों के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार वेद, नित्य और अविनाशी ज्ञान के भंडार हैं परंतु काल के पैमाने पर तब प्रकट होते हैं जब मानव इतनी प्रगति कर लेता है कि उसका दर्शन कर सकने की योग्यता के ऋषि संसार में आ जाते हैं। इसलिए अनन्त ज्ञान के भंडार भी लगभग 10 हजार वर्ष पूर्व प्रकट हुए। वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों का सार गीता है। भगवान् ने कहा है कि यह ज्ञान अविनाशी है जो संसार से लुप्त हो गया था इसलिए इसे पुन: कह रहा हूँ (4.1-3)। इतिहास के पैमाने पर देखें तो लगभग 5200 वर्ष पूर्व ईश्वरीय वाणी के रूप में गीता प्रकट हुई और वेदव्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई।
गीता के समय समाज में प्रचलित धार्मिक परिस्थितियाँ –
उस समय समाज में कर्मकाण्डों का बड़ा जोर था। उपनिषदों का विचार भी ताजा ताजा आया था। दोनों के बीच बड़ा संघर्ष था। कर्मकांडी यज्ञ, अनुष्ठान आदि के द्वारा स्वर्ग सुख की कामना करते थे जबकि ज्ञानमार्गी स्वर्ग को संसार की तरह अस्थाई मानते थे और शाश्वत सुख की खोज पर जोर देते थे। उस समय कर्मकांड बहुत बढ़ गये थे । राजा लोग बड़े-बड़े यज्ञ जैसे राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेय आदि के द्वारा अपना प्रभुत्व दिखाते थे। यह मान्यता समाज में स्थापित हो गई थी कि यज्ञ करने से जीवन में धन-धान्य की प्राप्ति होगी और जीवन के बाद स्वर्ग मिलेगा। इसके विपरीत ज्ञान के नाम पर संसार से पलायन करके गहन वनों में जाकर तप करने की प्रवृत्ति बढ़ी थी। सामान्य जन जो जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहे हों व भला इन मँहगे, ताम-झाम वाले यज्ञों को कैसे कर सकते थे वे संसार को छोडक़र वन में पलायन भी नहीं कर सकते थे। आम व्यक्ति के लिए अपने उद्धार का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता था। तब श्रीकृष्ण ने गीता के माध्यम से क्रांति ला दी। उन्होंने कहा कि अपने अपने काम में लगा हुआ मनुष्य, अपने कर्मों से ही भगवान् का पूजन कर सिद्धि प्राप्त करता है (18.45,46) । इस प्रकार अब कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं रहा। यदि खेती करता किसान, व्यापार करता व्यापारी, विद्यादान करता गुरु, युद्ध लड़ता सैनिक अपने कर्मों को भगवान् को अर्पित कर देता है तो वह भी ईश्वर की पूजा है।
गीता में हर अध्याय साधना का प्रगतिशील स्तर है –
सामान्य रूप से गीता की व्याख्या श्लोकों के अर्थ के विस्तार के रूप में की जाती है। इससे प्रत्येक श्लोक एकाकी हो जाता है व गीता, विभिन्न विचारों का गुलदस्ता, जिसमें प्रत्येक फूल का रूप, रंग और गंध एक-दूसरे से अलग है, लगने लगती है। इसलिए गीता को समझने में पाठक भ्रमित हो जाता है। परंतु गीता को समग्रता में अध्ययन करने से पता चलता है कि गीता, प्रथम से अठारहवें अध्याय तक गीतोक्त साधना के प्रगतिशील स्तर बताती है। गीता विभिन्न पुष्पों का गुलदस्ता नहीं बल्कि नदी की धारा दिखाई देती है जिसमें लहरें, भँवर, प्रपात तो हैं परन्तु उनमें व्याप्त, उनका आधार, जल स्पष्ट दिखाई देने लगा है।
गीता की जिज्ञासा का उद्भव –
संसार में अधिकतर लोग शरीर, प्राण और इन्द्रियों से बद्ध जीवन जीते हैं जिसे सांसारिक जीवन कहते हैं। वे इससे आगे सोच ही नहीं पाते। महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन भी ऐसा ही जीवन जीता रहा था। अभी तक उसके सारे कार्य सांसारिक कामनाओं – सम्मान, धन, राज्य, परिवार आदि – की पूर्ति के लिए थे। अर्जुन उस समय का श्रेष्ठ योद्धा और विचारवान् विद्वान था जिसे अब तक जीवन का अनुभव हो चुका था। उसने पाया था कि उक्त सांसारिक उपलब्धियाँ जीवन में स्थाई सुख व शांति नहीं ला सकतीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि युद्ध जैसे घोर कर्म से होने वाले पाप और स्वजनों के बिछोह से होने वाले दु:ख से वह कैसे बच सके। उसके मन में व्यक्तगित, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों को लेकर भीषण संघर्ष छिड़ा था।
अब तक के शास्त्रीय और धार्मिक विधान उसकी इस आंतरिक समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वह युद्ध छोडक़र पलायन करने, भिक्षा माँगने का निश्चय करने लगा था। गीता को समझने के लिए पहले अर्जुन की मानसिकता की इस पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। जब तक हम विचारहीन तरीके से सांसारिक जीवन जी रहे हैं तब तक न तो गीता की जरूरत महसूस होती है और न ही गीता समझ में आती है। धार्मिक और नैतिक जीवन जीते हुए, अपने पुरुषार्थ से सांसारिक उपलब्धियाँ अर्जित करते हुए जब यह अनुभव होता है कि यह जीवन स्थाई तृप्ति नहीं दे रहा तब जीवन में आध्यात्मिक पिपासा जागती है तब गीता समझने की जिज्ञासा पैदा होती है।
गीता को कैसे समझें –
गीता केवल मस्तिष्क से पूरी तरह समझ में नहीं आती। उसके लिए स्वच्छ हृदय की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने जीवन में आहार, विहार, कर्म, सोना, जागना आदि में युक्तियुक्तता और नियमितता (6.16,17), यम जैसे सत्य अहिंसा अपरिग्रह आदि और नियम जैसे शुद्धि, संतोष, ईश्वर पर विश्वास आदि गुणों का विकास करना आवश्यक है। एक अपराधी, दुष्ट, अत्यंत पापी भी अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, वह विज्ञान पढ़ा सकता है परंतु ऐसा व्यक्ति गीता नहीं समझ सकता है न समझा सकता है। गीता समझने के लिए संत का हृदय और शांत मस्तिष्क की जरूरत होती है। गीता केवल भाष्य पढऩे से भी समझ में नहीं आती। गीता तो शुद्ध अध्यात्म विज्ञान है। उसकी व्याख्या अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि अनेक रूपों में की गई है। यह व्याख्या करने वाले महापुरुष की चेतना की स्थिति और उस युग की आवश्यकता पर निर्भर करती है। हमारे जीवन की आवश्यकता सबसे अच्छी तरह हमें स्वयं पता होनी चाहिए। इसलिए उस आवश्यकता के अनुरूप गीता की कौन सी व्याख्या ठीक है हम तय करके उस दिशा में बढ़ सकते हैं।
ईश्वर का गीत होने के कारण गीता विश्व के सभी मानवों के लिए संदेश देती है। इसलिए अच्छा यह है कि हम श्रद्धा से गीता का पाठ करें और प्रत्येक श्लोक को देवता मानकर उससे अपना अर्थ हमें देने की प्रार्थना करें। यह साधना बगैर उकताए हुए, निरंतर करते रहें (6.23)। गीता भगवान् का वांगमय स्वरूप है। जब हमारे हृदय की पात्रता बन जाएगी तब गीता की कृपा होगी और हमारे अनुकूल अर्थ भीतर से प्रकट हो जाएगा जो हमारे जीवन को बदल देगा।
दिग्गज चाहते है जब जिम्मेदारी हमारी तो पसंद भी हमारी होना चाहिए